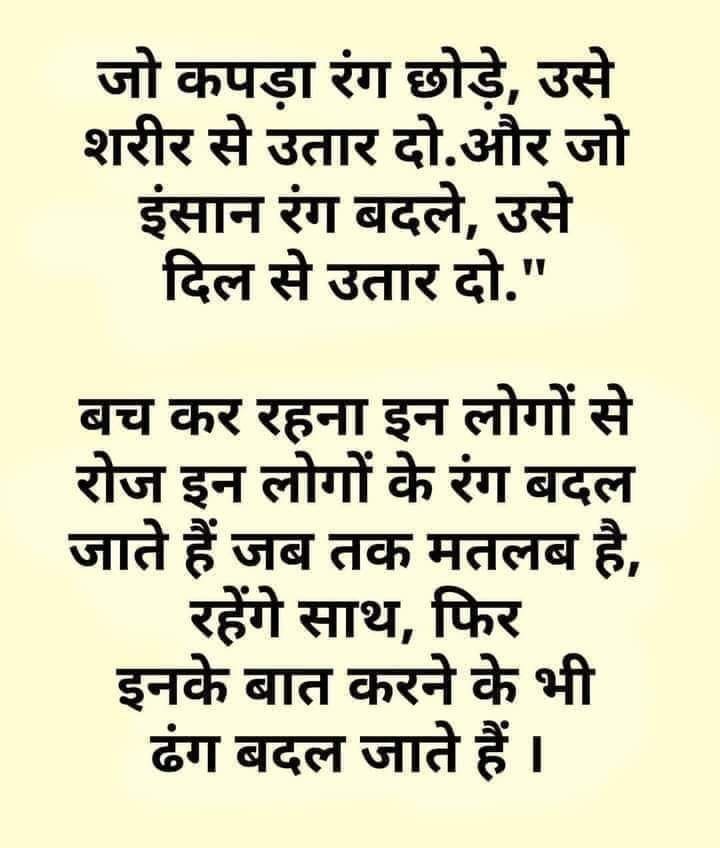🙏 जय ऋष्यराज 🙏
Articles: समाज का ऋण चुकाना ही चाहिए, मगर इस बात का ध्यान रखें कि आपके द्वारा चुकाएँ ऋण का उपयोग “सेवा धर्म” वाले कर रहे हैं या “मेवा धर्म” वालों द्वारा किया जा रहा हैं…!
〰〰➖🌹➖〰〰 〰〰➖🌹➖〰〰 〰〰➖🌹➖〰〰 〰〰➖🌹➖〰〰 〰〰➖🌹➖〰〰
👉 एक मनुष्य पर समाज का कितना ऋण है, यह सही-सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता, कुछेक बातों के लिए ही हम विचार करें, तो पता चलेगा कि समाज का यह ऋण भी इतना भारी है, कि उसे चुकाने के लिए कितने ही जन्म लेने पड़ेंगे…?
जो भोजन हम खाते हैं, जो वस्त्र हम पहनते हैं, जो पुस्तकें हम पढ़ते हैं, तथा नित्यप्रतिदिन के जीवन में जिन वस्तुओं का उपयोग हम करते हैं, उसमें कितने ही मनुष्यों का श्रम व सहयोग लगा हुआ है…!
एक माचिस की डिब्बी पचास पैसे में मिलती है, जिससे पचास बार आग जलाई जा सकती है, पचास पैसे कमाने में मुश्किल से पाँच या दस मिनट लगते होंगे, लेकिन वही डिब्बी हम पूरा दिन लगाकर भी नहीं बना सकते, विचार किया जाना चाहिए कि एक माचिस की डिबिया के लिए ही हम समाज के कितने ऋणी हैं…?
मनुष्य ने विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति की है, जो असाधारण लाभ उठाये हैं, तथा जिनके बल पर मनुष्य सृष्टि का मुकुटमणि बना हुआ है, वह समाज का ही अनुदान है, निजी पुरुषार्थ तो उन उपलब्धियों में नगण्य ही समझा जाना चाहिए…!
👉 जिस समाज का इतना उपकार और अनुदान लेकर मनुष्य सुख-सुविधाएँ प्राप्त करता है, उसका वह ऋणी है, इस ऋण को चुकाना कृतज्ञता की, प्रत्युपकार की और सामाजिक श्रृंखला की परंपरा बनाये रखने की दृष्टि से नितांत आवश्यक है, यदि लोग समाज के कोष से लेते तो रहें, पर उसका भंडार भरने की बात न सोचें, तो वह सामूहिक कोष खाली हो जायगा, समाज खोखला और दुर्बल हो जाएगा, उसमें व्यक्तियों की सुविधा बढ़ाने एवं सहायता करने की क्षमता न रहेगी, फलतः मानवीय प्रगति का पथ अवरुद्ध हो जायगा…!
“प्राप्त तो करें पर लौटायें नहीं” की नीति अपना ली जाए तो बैंक दिवालिये हो जायेंगे, सरकार खोखली हो जायगी, जमीन का उपार्जन बंद हो जायेगा, व्यापार की श्रृंखला ही बिगड़ जायेगी, इस संसार में “लो” (आदान) और “दो” (प्रदान) की नीति पर सारी व्यवस्था चल रही है…!
“लो” (आदान) के लिए तैयार “दो” (प्रदान) के लिए इनकार की परंपरा यदि चल पड़े तो सारा क्रम ही उलट जायगा, तब हमें असामाजिक आदिम युग की ओर वापस लौटना पड़ेगा…!
👉 आधा भाग मनुष्य की बुद्धि और श्रमशीलता का और आधा भाग सामाजिक अनुदान का माना गया है, तदनुसार तत्त्वदर्शियों ने यह व्यवस्था बनाई है कि उसे अपनी जीवन संपदा का आधा भाग अपनी शरीर यात्रा के लिए रखना चाहिए, और आधा सामाजिक उत्कर्ष के लिए लगा देना चाहिए, दूसरे शब्दों में इसे “सेवा धर्म” की प्रेरणा भी कहा जा सकता है, मनुष्य को ईश्वर ने इतनी विभूतियाँ दीं, इतने विशेष अधिकार दिये, उनके साथ जुड़े हुए दायित्वों की पूर्ति “सेवा धर्म” अंगीकार करने से ही संभव है…!
समाज का जो इतना भारी ऋण उसके ऊपर है, उससे आंशिक मुक्ति “सेवा धर्म” अपनाने से प्राप्त की जा सकती है, “सेवा धर्म” में यदि किंचिन्त मात्र भी स्वार्थ की भावना उत्पन्न हो जाये तो “सेवा धर्म” “मेवा धर्म” बन जाता हैं, व्यक्ति यदि “मेवा धर्म” के लिए काम करता हैं, तो उसे दर-दर भटक कर धनसंचय करना पड़ता हैं, क्यूँकि ऐसा करने पर हिसाब या काम दिखाने की जरूरत नही पड़ती, बस कुछ उपहार ओर लोकलुभावने सपने बेच कर आसानी से धनसंचय किया जा सकता हैं…!
👉 “मेवा धर्म” में मेवा पाने वालों को मिल बाँट कर “मेवा लाभ” मिलता हैं, सभी को “मेवा प्राप्त करने की योग्यता के आधार पर “फल” बाँटने पड़ते हैं, “बेर वाले को बेर” और “सेर (तोल) वाले को सेर” का लाभ पहुँचाये जाने पर ही “मेवा धर्म” वाले “सेवा धर्म” के नाम पर धनसंग्रह कर घर भर लेते हैं…!